बीटीसी एवं सुपरटेट की परीक्षा में शामिल शिक्षण कौशल के विषय समावेशी शिक्षा में सम्मिलित चैप्टर मन्द बुद्धि बालकों की पहचान, विशेषताएं, प्रकार, कारण / मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री आज हमारी वेबसाइट hindiamrit.com का टॉपिक हैं।
Contents
मन्द बुद्धि बालकों की पहचान, विशेषताएं,प्रकार,कारण / मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री
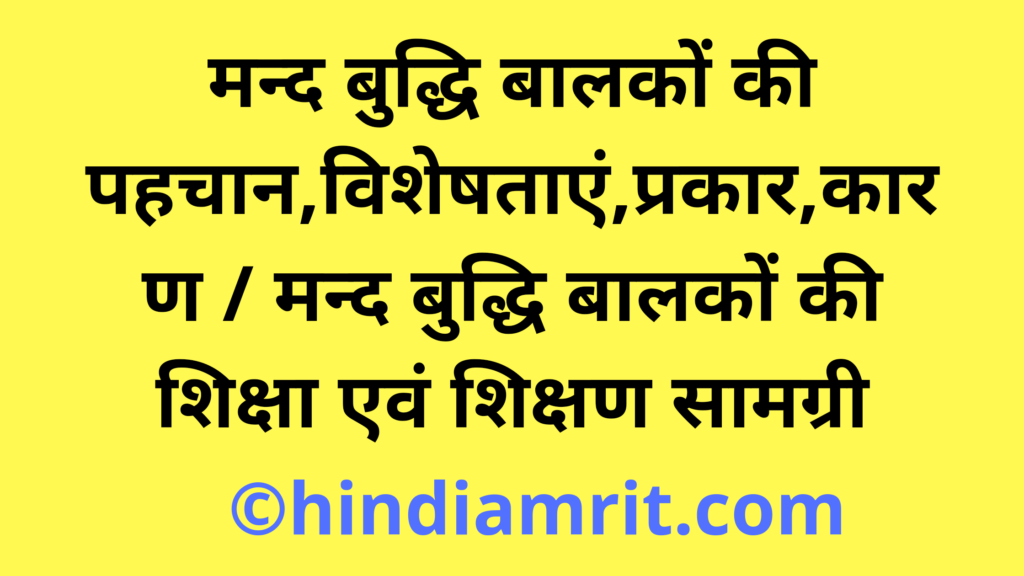
मानसिक दक्षता से वंचित बालक / मन्द बुद्धि बालकों की पहचान, विशेषताएं, प्रकार,कारण
Tags – मन्द बुद्धि बालक के प्रकार,मन्द बुद्धि बालकों का वर्गीकरण,मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा,Mandbuddhi balak ka arth aur paribhasha,मन्द बुद्धि बालकों के कारण बताइए,मन्द बुद्धि बालक का अर्थ,मन्द बुद्धि बालकों के कारण,मन्द बुद्धि बालकों की विशेषताएं, Mandbuddhi balak kise kahte hai,मन्द बुद्धि वाले बालकों की पहचान,मन्द बुद्धि के कारण,मन्द बुद्धि बालकों की पहचान,मन्द बुद्धि बालकों की समस्या,Mandbuddhi balak ki paribhasha,मन्द बुद्धि बालक की परिभाषा,मन्द बुद्धि के कारण,मन्द बुद्धि बच्चों की शिक्षा,मन्द बुद्धि बच्चों की पहचान,मन्द बुद्धि बच्चों के लक्षण,मन्द बुद्धि बालक के प्रकार होते हैं,Mandbuddhi balak ke prakar,मन्द बुद्धि के प्रकार,मन्द बुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं,मन्द बुद्धि छात्रों के लिए शिक्षण विधियों,मन्द बुद्धि बालकों के लिये शैक्षिक उपकरण,मन्द बुद्धि बालकों की पहचान,विशेषताएं,प्रकार,कारण / मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री
मानसिक दक्षता से वंचित बालक (मन्द बुद्धि बालक)
मानसिक दक्षता से वंचित या मन्द बुद्धि बालक वे होते हैं, जिनके सीखने की गति धीमी होती है और सीखकर भूल भी जाते हैं अर्थात् उनमें स्मरण क्षमता का अभाव होता है। ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, इनमें मौलिकता का अभाव होता है और नवीन समस्या पर विचार नहीं कर सकते। इनका व्यवहार असमायोजित होता है तथा समाज से पृथक् रहना चाहते हैं। इन्हें हताशा एवं निराशा का अनुभव होता है। ये सामान्य शिक्षण विधियों से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी मानसिक आयु कम होती है अर्थात् अपनी कक्षा और उससे भी नीचे की कक्षा का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर सकते।
इस प्रकार मन्द बुद्धि या मानसिक दक्षता से वंचित बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है, जो सामान्य आयु तथा सामान्य स्तर के कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। ये बालक परिवार, विद्यालय तथा समुदाय में समायोजित नहीं हो पाते तथा इनमें हीन भावनाएँ तथा हीन ग्रन्थियाँ (Inferiority complex) उत्पन्न हो जाती हैं। बुद्धि लब्धि की दृष्टि से 20 से कम बुद्धि लब्धि (I.Q.) वाले बालकों को मानसिक दृष्टि से पिछड़ा या मानसिक दक्षता से वंचित माना जाता है। प्रारम्भ में इन बालकों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था वरन् इनकी बुद्धिहीनता को पूर्व संस्कारों का प्रभाव कहकर भाग्य पर छोड़ दिया जाता था किन्तु इनकी ओर अब ध्यान गया है और उनका उचित प्रबन्ध होने लगा है।
पश्चिमी देशों में पिछड़ेपन की परिभाषा देने में तथा पता लगाने में शारीरिक आयु (C.A.), मानसिक आयु (M.A.) तथा शैक्षणिक आयु(E.Q.) आदि का प्रयोग किया गया है किन्तु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अभाव में तथा मानसिक आयु का ठीक-ठीक पता लगाने की असमर्थता के कारण हम पिछड़ेपन का पता लगाने में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अतः भारतीय बालकों के पिछड़ेपन की परिभाषा इस प्रकार की गयी है-“मानसिक रूप से मन्द बुद्धि या पिछड़ा बालक वह है जो एक या अधिक विषयों में बहुत कम काम कर रहा हो, यद्यपि उसकी आयु कक्षा की औसत आयु के लगभग बराबर हो।”
मंदबुद्धि बालक की परिभाषाएं
(1) मनोवैज्ञानिक बर्ट (Burt) के अनुसार-“पिछड़ा हुआ बालक वह है, जो शिक्षा सत्र (Session) के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक दर्जे नीचे का कार्य न कर सके अर्थात् मान लिया, एक बालक आयु की दृष्टि से आठर्वी कक्षा में होना चाहिये। यदि वह बालक आठवीं कक्षा के मध्य में सातवीं कक्षा का कार्य करने में असफल है तो वह पिछड़ा हुआ बालक कहा जायेगा। दूसरे दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ बालक वह है जिसकी शैक्षणिक लब्धि 85 या कम हो।”
(2) क्रो एंड क्रो के अनुसार,“ मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है,अतः उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंदबुद्धि बालक कहते हैं ।”
(3) जी डी पेज के अनुसार,“ मानसिक मंदता सामान्य या कम विकास की ऐसी अवस्था है जो बालक में बुद्धि संबंधी कमी या अक्षमता के लिए उत्तरदायी होती है ।”
मंदबुद्धि बालक के प्रकार / मानसिक अक्षमता के प्रकार / मानसिक मंदता के प्रकार
(1) छात्रों का कक्षा के कार्य के आधार पर
1. सामान्य पिछड़ापन (General backwardness)-जब कोई छात्र पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में असफल रहता है तो वह सामान्य रूप से पिछड़ा हुआ बालक कहा जाता हैं।
2. विशिष्ट पिछड़पन (Specific backwardness)-जब छात्र पाठ्यक्रम के किसी एक विषय या क्षेत्र (Area of knowledge) में पिछड़ा हुआ है तो वह विशिष्ट क्षेत्र या विषय में पिछड़ा हुआ होता है।
(2) सामान्य वर्गीकरण
(1) मन्दित मना बालक – ( बुद्धिलब्धि 70 से कम )
(2) धीमी गति से सीखने वाला बालक ( 70 – 85 बुद्धिलब्धि )
(3) बुद्धिलब्धि के आधार पर मंदबुद्धि बालक के प्रकार
(1) हीन बुद्धि बालक ( 70 – 89 बुद्धिलब्धि )
(2) मूर्ख बुद्धि बालक ( 59 – 69 बुद्धिलब्धि )
(3)मूढ़ बुद्धि बालक ( 25 – 49 बुद्धिलब्धि )
(4) जड़ बुद्धि बालक ( 0 – 24 बुद्धिलब्धि )
मन्द बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषताएँ
मन्द बुद्धि या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख विशिष्टताएँ या विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
(1) बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर पता लगा है कि इन बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर होती है। (2) ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते। अत: गणित, व्याकरण तथा विज्ञान आदि के अध्ययन में रुचि नहीं लेते। (3) परीक्षा में बार-बार अनुत्तीर्ण होते हैं, जिससे आयु के अनुसार छोटी कक्षा में ही पढ़ते हैं। (4) अपने संवेगों पर नियन्त्रण नहीं रख पाते। (5) ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। (6) इनमें आत्म-विश्वास का अभाव रहता है।
(7) ये सामाजिक कार्यों को करने के योग्य नहीं होते और अपने को सदैव अयोग्य, निरर्थक तथा अपूर्ण समझते हैं । (8) यदि इनसे बात करें तो ये कहते कम हैं,सुनते अधिक हैं। (9) इन बालकों की संकल्प शक्ति अत्यन्त निर्बल होती है। अत: ये किसी बात का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते। (10) ये सीमित एवं साधारण रुचियाँ लिये होते हैं। (11) इनमें मौलिकता का अभाव होता है तथा ये सामान्यीकरण करने में अयोग्यता रखते हैं। (12) इनका अनैतिकता और अपराध की ओर भी झुकाव हो जाता है।
मन्द बुद्धि के कारण / मानसिक मंदता के कारण
मन्द बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
(1) मस्तिष्क में कमियों के आ जाने से मानसिकदोष आजाता है। मस्तिष्क कोशिकाओंनको बुखार के कारण, घाव या चोट लगना भी मन्द बुद्धि का कारण है। अनेक और बीमारियाँ; जैसे-आईटिस, एनिसिफलाईटिस, कोन निजिन्थल सिफलिस तथा जर्मन मीसलस आदि भी मानसिक पिछड़ेपन के लिये उत्तरदायी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऐपीलैप्सी तथा अधरंग एपीप्लैप्सी आदि बीमारियाँ भी इस दोष को जन्म देती हैं।
(2) व्यक्तित्व, संवेग तथा अन्य तथ्यनबालक की निष्पत्ति पर प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ पिछड़ापन व्यक्तित्व सम्बन्धी दोषों पर भी निर्भर करता है। एफरन (Aphron) के अनुसार पढ़ने में पिछड़ापन संवेगात्मक दोषों के कारण होता है। कुछ बालकों में यह छिपा होता है और इसका मनोविश्लेषणात्मक विधि (Psycho-analytical method) से पता लगाया जा सकता है। एफरन के अनुसार निष्पत्ति-परीक्षण (Achievement tests) के साथ-साथ अन्य परीक्षणों का प्रयोग भी मानसिक अक्षमता के कारणों को पता चलाने के लिये करना चाहिये।
(3) यह विचार सदैव ही लोकप्रिय रहा है कि मानसिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है। इस पिछड़ेपन का मुख्य अंश बालकों क। उनके माता-पिता के मानसिक पिछड़ेपन से मिलता है। बुद्धिहीनता पूर्वजों में भी मिलती है और इसका हस्तान्तरण बालकों में भी हो जाता है। इसका कारण गुणसूत्रों का दोष होता है।
(4) जिन बालकों के घर का वातावरण दोषयुक्त रहता।है, उनमें भावना-ग्रन्थि विकसित हो जाती है। पढ़ने में रुचि न होने के कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण घर में द्वेष, लड़ाई-झगड़े आदि होना है। संवेगों पर नियन्त्रण न कर पाने पर मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है और बालक कहीं भी समायोजन नहीं कर पाता।
(5) विद्यालय भी बालकों में पिछड़ेपन को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित प्रकार से हैं-(i) बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान न देना। (ii) जो बालक बीमारी या अन्य कारणों से विद्यालय से उपस्थित रहते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। अंत: उन पर विशेष ध्यान देकर उनके पिछड़े कार्यों को पूरा नहीं कराया जाना । (iii) जब बालकों को रोचक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जाता तो वे पाठ को नहीं समझ पाते और अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं।
उपरोक्त कारकों में से कोई भी कारक मानसिक पिछड़ेपन या मन्द बुद्धिपन को उत्पन्न।करने के लिये क्रियाशील हो सकता है।
मन्द बुद्धि पहचान की विधियाँ
मन्द बुद्धि या पिछड़े बालकों की पहचान की विधियाँ अनलिखित हैं-
1. अध्यापक द्वारा निरीक्षण-कक्षा का अध्यापक बालकों के बारे में अधिक जानकारी रखता है। वह यह देख सकता है कि कौन बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है और क्यों पिछड़ा है?
2. निष्पत्ति-परीक्षण-सभी स्तरों पर निष्पत्ति-परीक्षण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ साधारण अध्ययन के लिये हैं जबकि कुछ शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाने के लिये हैं। अध्यापक को यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन-से परीक्षण प्रयोग में लाये जायें।
3. बुद्धि-परीक्षण-मानसिक अक्षमता की पहचान के लिये बुद्धि-परीक्षण भी अनिवार्य है क्योंकि शैक्षिक पिछड़ापन प्राय: बुद्धि की कमी के कारण होता है।
4. व्यक्तित्व-परिसूची-व्यक्तित्व-परिसूचियों से व्यक्तित्व एवं प्रेरणा का पता लगता है तथा प्रेरणा की कमी का भी पता लगता है।
5. केस अध्ययन-इससे बालक के परिवार तथा घर का पता लगता है, जो बालक के विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।
6. शारीरिक तथा इन्द्रिय परीक्षाएँ-यद्यपि सभी बालकों की शारीरिक एवं इन्द्रिय परीक्षाएँ की जाती हैं परन्तु शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक की परीक्षा विशेषतः ध्यानपूर्वक करनी चाहिये। इस प्रकार के परीक्षणों में हाथों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बैट्स (Betts) के अनुसार, प्रत्येक हाथ से कागज-पेंसिल पर अनेक टेपिंग (Tapping) परीक्षण करवाने चाहिये, पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से लिखवाना चाहिये, प्रक्षेपण (Throws) तथा इसी प्रकार के परीक्षण लेने चाहिये, कैंची का प्रयोग करवाना चाहिये और वस्तुओं को पकड़ने की शक्ति देखनी चाहिये। बैट्स एक कागज के छेद से देखने पर भी बल देता है जिससे यह पता चलता है कि कौन-सी आँख अधिक देखने पर बल देती है? टेलीबिनोकुलर (Telebinocular) परीक्षण से आँखों के दोष के विषय में पता लगता है।
मानसिक रूप से मन्द या पिछड़े बालकों की शैक्षिक व्यवस्था
मानसिक रूप से विकलांग अथवा अतिमन्द बालकों की बुद्धि-लब्धि सामान्यतया 70 या उससे नीचे होती है। सामान्य बालकों के साथ में अध्ययन नहीं कर पाते । इसलिये बड़े नगरों.में ऐसे बालकों के लिये अलग विद्यालय स्थापित होने लगे हैं। सामान्य बालकों के साथ और.भी अधिक पिछड़ जायेंगे। इसलिये अलग कक्षा लगायी जा सकती हैं। इन बालकों को स्नेह एवं सहानुभूति वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिये। मन्द बुद्धि बालक चार प्रकार के होते हैं-
(1) जड़ बुद्धि (Idiots)- इनकी 0-24 तक बुद्धि-लब्धि होती है। (2) मूढ़ बुद्धि (Impeciles)-इनकी 25-49 तक बुद्धि-लब्धि होती है। (3) मन्द बुद्धि (Morons)- इनकी 50-70 तक बुद्धि-लब्धि होती है। (4) सामान्य बुद्धि-इनकी 70-80 तक बुद्धि-लब्धि होती है।
इन बालकों के लिये सर्वप्रथम फ्रांसीसी चिकित्सक डॉ. इटाई ने और इसके उपरान्त सैगविन ने अध्ययन किया। इसके बाद अन्य देशों में भी काम हुआ। इन बालकों की शिक्षण.के सम्बन्ध में किर्क तथा जॉनसन ने निम्नलिखित उद्देश्य बताये हैं-
(1) इनमें न्यूनतम शिक्षा.सम्बन्धी योग्यता का विकास करना; जैसे-पढ़ना, लिखना,और साधारण गणित। (2) उनमें ऐसी क्षमता विकसित करना है ताकि वे विश्राम के क्षणों में विभिन्न क्रियाकलापों से अपना मनोरंजन कर सकें। (3) ऐसे बालकों में व्यावसायिक कौशलों का विकास करना। (4) उन्हें इस योग्य बनाना कि वे परिवार सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को वहन कर सकें। (5) इन बालकों में ऐसी आदतों का विकास करना, जिससे कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। (6) उनमें ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे सामुदायिक कार्यक्रमों में एक क्रियाशील एवं उपयोगी सदस्य के रूप में भाग ले सकें।
मानसिक रूप से विकलांग या पिछड़े बालकों के शैक्षिक समावेशन हेतु उनकी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित होना चाहिये-
(1) ऐसे बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा जीवन निर्वाह भली-भाँति कर सकें। अत: हस्तकला या दस्तकारी की व्यावसायिक शिक्षा देना अपेक्षित है। ये बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं इसलिये उनमें समायोजन की।भावना का विकास करना आवश्यक है। समाज में भली-भाँति समायोजन के लिये उनकी।भाषायी क्षमता का विकास किया जाना चाहिये। सामान्य एवं प्रतिभावान बालकों के साथ।सम्पर्क बनाये रहने से इनकी मानसिक मन्दता कम होती है और सामाजिक तथ्यों का ज्ञान होता है। विशेष रूप से ऐसे बालकों के लिये पृथक् विद्यालयों अथवा कक्षाओं की आवश्यकता।रहती है।
(2) मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिये पर्याप्त पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होनी चाहिये। इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिकाधिक खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिये। विभिन्न पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी उनमें समायोजन एवं आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती है।
(3) सामान्य बालकों से इनका पाठ्यक्रम पृथक् होता.चाहिये। इनकी शिक्षा में लेखन, पठन तथा अंकगणित पर विशेष ध्यान देना चाहिये। लेखन में वर्ण-विन्यास जानना, पत्र लिखना तथा प्रार्थना पत्र लिखना आदि पर अधिक बल देना चाहिये। पठन में वस्तुओं, सड़कों, गलियों, नगरों, मूल्यों, सूचियों को जानने तथा अपने परिवार एवं पास-पड़ोस की वस्तुओं से परिचय पाने आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक जीवन से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है और समायोजन में सफलता मिलती है।
उन्हें सहानुभूति से समझाना चाहिये कि वे दिन-प्रतिदिन के कार्यों को भली-भाँति सम्पन्न कर सकते हैं। परिवार के लिये वस्तुएँ खरीदने तथा उनका हिसाब-किताब लगाने आदि का ज्ञान भी सिखाना आवश्यक है। इनका पाठ्यक्रम व्यवसाय आधारित एवं व्यावहारिक होना चाहिये।।इनको पढ़ाने वाले अध्यापक ऐसे होने चाहिये जिनमें सहानुभूति, स्नेह एवं समायोजन की।भावना हो और वे संवेगात्मक रूप से सन्तुलित हों। ऐसे बालक किसी भी बात को अनेक बार।समझाने पर समझ पाते हैं। अत: ऐसे अध्यापक हों जो इन बालकों पर क्रोधित न होते हों अपितु बार-बार प्रेम से समझाते हैं।
(4) मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षण व्यवस्था में आवासीय विद्यालय भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होते हैं। आवासीय विद्यालयों में बालकों को निर्देशन देने के।लिये एक अच्छी योजना बनायी गयी है। आवासीय विद्यालयों में सही वातावरण एवं सही।निर्देशन दिया जा सकता है। उपकरणों की सम्पूर्ण सुविधाएँ होती हैं।
(5) इन बालकों की चिकित्सकों द्वारा जाँच भी विद्यालय में नियमित रूप से बराबर होनी चाहिये क्योंकि इससे।इनकी सही स्थिति का पता चलता रहेगा और आवश्यक परामर्श, निर्देशन आदि भी समय-समय पर दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक मनोवैज्ञानिक का भी बराबर परामर्श लेना चाहिये, जिससे वे कुसमायोजित होने से बच जायें। इसके साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक परामर्शदाता एवं निरीक्षकों का भी बालकों के साथ सहयोग आवश्यक है, इन बालकों को परिवार, विद्यालय, पड़ोस एवं साथियों से पूर्वाग्रहों से बचाना चाहिये क्योंकि ऐसे बालकों के बारे में पागल तथा मूर्ख आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
(6) इनकी शिक्षण व्यवस्था में सहायक सामग्री का अपना विशेष महत्त्व है क्योंकि इनकी बुद्धि-लब्धि कम होती है। इसलिये केवल शाब्दिक वर्णन या भाषण से भली-भाँति किसी तथ्य को समझ नहीं सकते। अध्यापकों को इनके लिये प्रयुक्त शिक्षण सामग्रियों की जानकारी होनी चाहिये। दृश्य-शृव्य सामग्री को समुचित प्रयोग कर दिखाकर अनुभव द्वारा समझने का प्रयास किया जाना चाहिये।
(7) शैक्षिक भ्रमण द्वारा ज्ञान को वास्तविक रूप से दिखाकर समझा सकते हैं। इनके शिक्षण में किसी विषय की बार-बार पुनरावृत्ति की जाय एवं अभ्यास कराया जाय तब उनकी समझ में यह तथ्य आ सकेगा।
मन्द बुद्धि छात्रों के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री
मन्द बुद्धि छात्रों के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री का स्वरूप खेल एवं अभिनय आधारित हो सकता है। विविध प्रकार के खेलों एवं चित्रों के माध्यम से उनको ज्ञान कराया जा सकता है। इसमें कविताओं का प्रयोग करके भी छात्रों का शिक्षण किया जाता है; जैसे-गिनती प्रारम्भ करने के लिये अँगुलियों का प्रयोग एवं शरीर के अंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इनके लिये चित्र एवं चार्ट बहुत उपयोगी होते हैं।
आपके लिए महत्वपूर्ण लिंक
टेट / सुपरटेट सम्पूर्ण हिंदी कोर्स
टेट / सुपरटेट सम्पूर्ण बाल मनोविज्ञान कोर्स
Final word
आपको यह टॉपिक कैसा लगा हमे कॉमेंट करके जरूर बताइए । और इस टॉपिक मन्द बुद्धि बालकों की पहचान, विशेषताएं, प्रकार, कारण / मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिये ।
Tags – मन्द बुद्धि बालक के प्रकार,मन्द बुद्धि बालकों का वर्गीकरण,मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा,Mandbuddhi balak ka arth aur paribhasha,मन्द बुद्धि बालकों के कारण बताइए,मन्द बुद्धि बालक का अर्थ,मन्द बुद्धि बालकों के कारण,मन्द बुद्धि बालकों की विशेषताएं, Mandbuddhi balak kise kahte hai,मन्द बुद्धि वाले बालकों की पहचान,मन्द बुद्धि के कारण,मन्द बुद्धि बालकों की पहचान,मन्द बुद्धि बालकों की समस्या,Mandbuddhi balak ki paribhasha,मन्द बुद्धि बालक की परिभाषा,मन्द बुद्धि के कारण,मन्द बुद्धि बच्चों की शिक्षा,मन्द बुद्धि बच्चों की पहचान,मन्द बुद्धि बच्चों के लक्षण,मन्द बुद्धि बालक के प्रकार होते हैं,Mandbuddhi balak ke prakar,
मन्द बुद्धि के प्रकार,मन्द बुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं,मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए,मन्द बुद्धि बच्चों की शिक्षा,मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था,मन्द बुद्धिता के कारण,मन्द बुद्धि बालकों की पहचान,मन्द बुद्धि बालकों का वर्गीकरण,मन्द बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है,मन्द बुद्धि छात्रों के लिए शिक्षण विधियों,मन्द बुद्धि बालकों के लिये शैक्षिक उपकरण,मन्द बुद्धि बालकों की पहचान,विशेषताएं,प्रकार,कारण / मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री